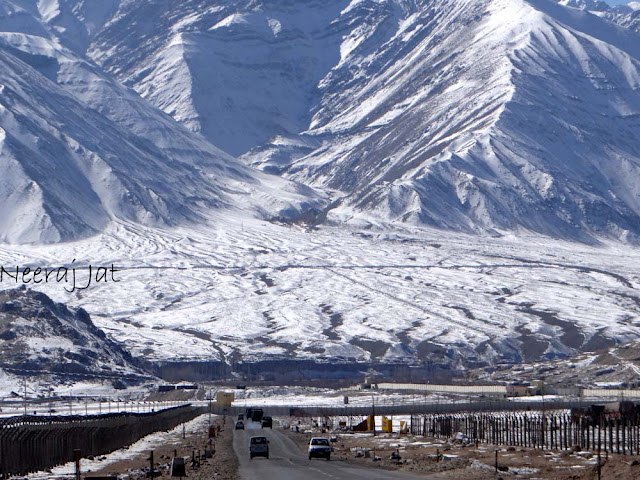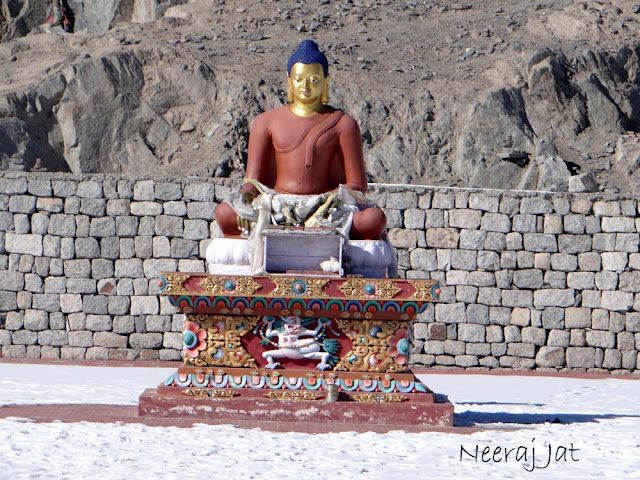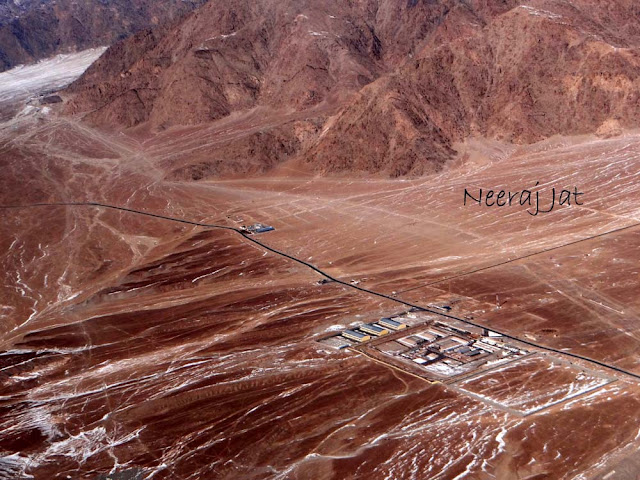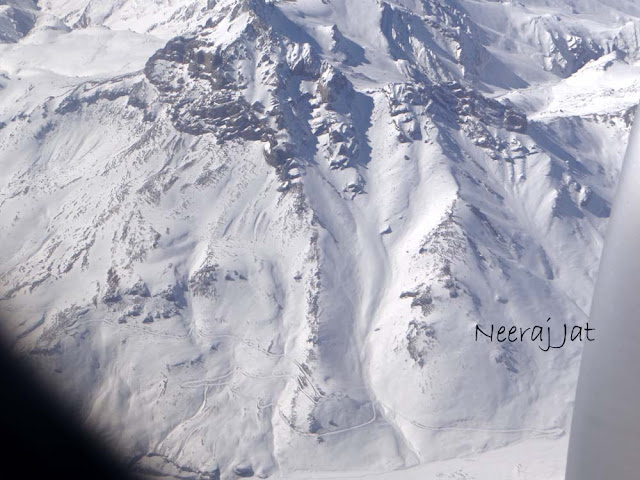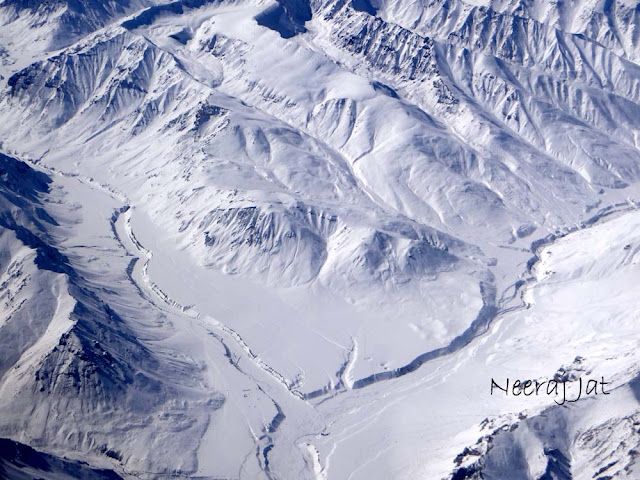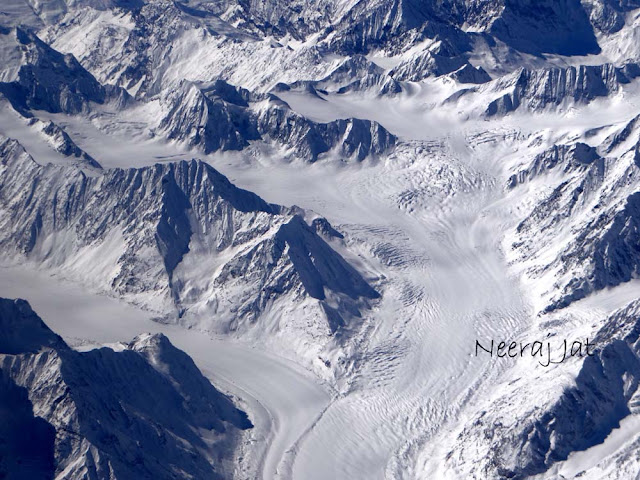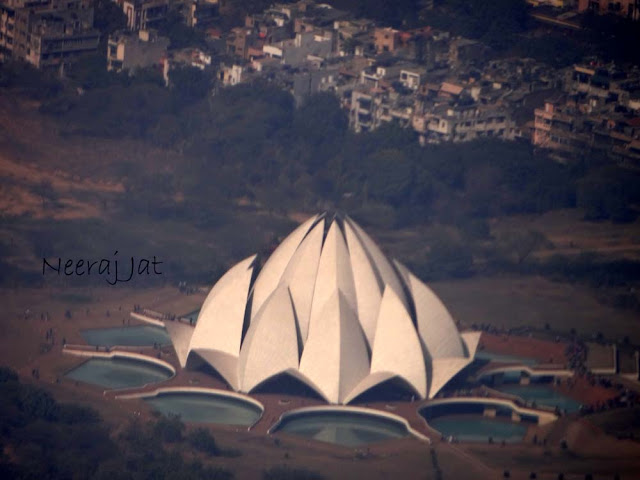मैं और रोहित ट्रेन से दोपहर होने तक कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके मैसेज हमारे मोबाइल पर अक्सर आते रहते थे। जब उनके यहां पहुंचे तो उनके वचन सुनकर पैरों तले से जमीन हिल पडी। बोले कि दो सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और आधी सैलरी भी एडवांस में लेंगे। बताया गया कि उस कम्पनी में आपको पांच हजार मिलेंगे, इसलिये ढाई हजार रुपये आपको अग्रिम जमा कराने होंगे। हमने मना कर दिया कि हम आपसे बात करके ही यहां आये हैं, आपने दो सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की ही बात की थी, आपको ढाई हजार रुपये के बारे में भी बताना चाहिये था। खैर, आखिरकार इस शर्त के साथ हमें उन्होंने इंटरव्यू लेटर दे दिया कि आप कम्पनी में भर्ती होते ही ढाई ढाई हजार रुपये का भुगतान कर दोगे।
अगले दिन दोनों सीधे गुडगांव पहुंचे। यह सोना ग्रुप की सोना सोमिक नाम की एक कम्पनी थी जिसकी मालिक करिश्मा कपूर हैं। इसमें लिखित तो नहीं हुआ लेकिन तीन बार इंटरव्यू हुए। कुल तीन जने वहां पहुंचे थे, तीनों को भर्ती कर लिया गया। और अगले दिन से ही कार्यभार संभालने को कहा जिसे हमने आसानी से दो दिन बाद करवा लिया ताकि गाजियाबाद और नोयडा से सामान गुडगांव शिफ्ट किया जा सके।
यह कम्पनी मेरे अनुकूल थी क्योंकि इसमें बडी बडी मशीनों पर मैकेनिकल काम होता था।
यहां जर्मनी से एक बेहद विशाल मशीन मंगाई गई थी जिसका आधा हिस्सा जो कि तकरीबन दस फीट था, जमीन के अन्दर था और शेष आधा जमीन के ऊपर। मशीन अभी आई ही थी, इंस्टाल नहीं हुई थी। हमें तीन शिफ्टों में इसी मशीन को चलाना था। दो महीने बाद जर्मनी से इसके इंजीनियर आयेंगे और इसे इंस्टाल करेंगे। तब तक हमें करना-धरना कुछ नहीं था, बस यहां आकर समय काटना था।
नोयडा की डेकी के मित्र याद आ रहे थे, जिनसे हमेशा बेहतरीन तालमेल बना रहा। एक बार समय निकालकर मैंने वहां जाकर नाइट ड्यूटी भी की और सबको बता दिया कि मैं अमित वर्मा के चंगुल से आजाद हो गया हूं। मेरा समकक्ष जो उस दिन नाइट ड्यूटी कर रहा था, उसने मुझे आजाद होने की बधाई दी और मेरे अच्छे नसीब की भी तारीफ की। साथ ही अपनी बदनसीबी को भी कोसने लगा। मैंने कहा कि दोस्त, नसीब ऊपर से बनकर नहीं आता, नीचे आकर खुद बनाया जाता है।
वो आज पांच साल बाद भी उसी कम्पनी में उसी पोस्ट पर उसी अमित वर्मा के नीचे काम कर रहा है।
गुडगांव में इस कम्पनी में जो माहौल मिला, वो जिन्दगी का एक बेहतरीन माहौल था। पहली बार हरियाणा में आया था, माहौल भी पूरी तरह हरियाणवी था। यही से मेरी बोली में हरियाणवी पुट आया।
हम तीनों को भर्ती तो सीधे कम्पनी ने किया था, लेकिन हमारी बागडोर सौंप दी गई एक ठेकेदार के हाथ में। कहने लगे कि दो तीन महीनों में तुम्हें नियमित कर दिया जायेगा। हम ‘इंजीनियरों’ को यह बात बडी चुभती थी।
हमें चूंकि निकट भविष्य में कोई उत्पादन नहीं करना था, कोई मशीन नहीं चलानी थी, इसलिये हफ्ते भर में ही हमें शिफ्ट की ड्यूटियों में लगा दिया गया। हमारा प्रोडक्शन मैनेजर (नाम भूल गया हूं) करीन 55 साल का था और उसने अपनी पूरी जिन्दगी यहीं पर लगा दी थी। वो आईटीआई का सर्टिफिकेटधारी था, इसलिये हम ‘इंजीनियरों’ की बेहद इज्जत करता था। चूंकि वो पढाई के मामले में हमसे पीछे था, इसलिये कभी भी उसने हमपर यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो हमारा बॉस है।
यहां ड्यूटी की टाइमिंग बडी खतरनाक थी। पहली शिफ्ट सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक, दूसरी शाम चार बजे से रात एक बजे तक और तीसरी यानी नाइट शिफ्ट रात एक बजे से सुबह आठ बजे तक होती थी। गनीमत थी कि गुडगांव बस अड्डे से कम्पनी तक लाने-ले जाने के लिये कम्पनी की बस चलती थी। हम जनवरी के आखिर में वहां भर्ती हुए थे, इसलिये सर्दियों भर रात बारह बजे रजाई से उठना बडा भयंकर काम होता था। मैं और रोहित साथ ही रहते थे। हममें से जिसकी भी नाइट ड्यूटी होती थी, वो बारह बजे उठकर सबसे पहले रोया करता था।
मार्च में जर्मनी और फ्रांस से कुछ इंजीनियर आये मशीन को इंस्टाल करने। खूब माथापच्ची कर ली, खूब दिमाग लगा लिया, खूब नक्शे देख लिये लेकिन कभी भी मशीन को अपने अनुकूल नहीं बना पाये। मशीन ने कसम खा ली कि नहीं चलूंगी। आखिरकार यूरोपियन इंजीनियर मशीन को छोड-छाडकर भाग गये।
हम पिछले करीब दो महीनों से कुछ नहीं कर रहे थे। हमारी भर्ती उसी मशीन को चलाने के लिये हुई थी, लेकिन अब फिर मामला अनिश्चित काल के लिये अटक गया। हम भी इन दो महीनों में बुरी तरह खाली आना-जाना करते हुए थक गये थे। ड्यूटी आते ही नींद आने लगती। सोने के लिये बडी शानदार जगह ढूंढी- कुर्सी वाला शौचालय। अन्दर से कुंडी लगाई, कुर्सी पर बैठे, पीछे कमर लगाई और सो गये। हमें कोई नहीं ढूंढता था। कुर्सी वाले शौचालय में कोई हरियाणवी भी नहीं आता था।
हां, एक बात रह गई। हम दोनों पर प्लेसमेंट एजेंसी वालों के ढाई ढाई हजार रुपये थे। भर्ती होते ही उन्होंने हम पर दबाव देना शुरू कर दिया। कम्पनी से निकलवा देने की धमकी देने लगे। हम पहुंचे सीधे एचआर डिपार्टमेंट में। उन्होंने बताया कि कोई जरुरत नहीं है उन्हें पैसे देने। हम बार बार किसी एजेंसी के कहने पर किसी को बाहर या अन्दर नहीं किया करते। आखिरकार, हमारे पांच हजार रुपये बच गये।
नोयडा वाली कम्पनी के अधिकारियों को पता चल गया था कि मैं गुडगांव में नौकरी कर रहा हूं, मेरा वहां तीन साल का अनुबन्ध था। मेरे पास फोन आया कि हम कानूनी कारवाही करेंगे। मैंने कहा कि कानूनी कारवाही तो कर लेना, लेकिन पहले अमित वर्मा से बात भी कर लेना। एक नालायक के तीन महीने की अतिरिक्त सैलरी लिये बिना चले जाना उनके लिये फायदे का सौदा ही था। वे भला क्यों मुझे दोबारा बुलाते?
हालांकि यह बडा आकर्षक लगता है कि बिना कुछ करे धरे और बिना किसी जिम्मेदारी के नौकरी चल रही हो, तो कौन इसे छोडकर जाना चाहेगा? लेकिन यही हमारे छोडकर जाने का कारण बना। हम यहां बुरी तरह बोर हो चुके थे। आठ घण्टे काटना धैर्य का जबरदस्त इम्तिहान था।
और एक दिन यहां से भी छोड दी।
गुडगांव में हम नौकरी-नौकरी खेला करते थे। जब चाहा जिस इलाके में चाहा नौकरी कर सकते थे। बस शर्त थी कि सैलरी कम्पनी की मर्जी से मिलेगी, ना कि आपकी मर्जी से। हमारी सैलरी कभी भी छह हजार से ज्यादा नहीं हुई।
सोना कम्पनी से छोडने के बाद रुख किया मानेसर का। मानेसर गुडगांव से करीब बीस किलोमीटर आगे एक औद्योगिक नगर है। बडी प्रतिष्ठित कम्पनी थी, नाम भूल गया हूं, सैलरी थी आठ हजार।
इंटरव्यू के लिये करीब बीस लडके आये थे। मेरे अलावा सब सज-धजकर। प्रतिष्ठित कम्पनी, अच्छी सैलरी और इतने ज्यादा प्रतियोगी। दो राउंड का इंटरव्यू हुआ, मेरा सलेक्शन हो गया। आज मैं बेहद खुश था क्योंकि यह मेरी चौथी कम्पनी थी और इतना कम्प्टीशन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। खुशी तो बनती ही है जब आप बीस लडकों को पछाडकर आगे निकलते हो।
यहां काम करने वाले सब डिप्लोमची ही थे। ध्यान नहीं कि इसमें क्या बनता था। पहले दिन जब कम्पनी पहुंचा तो गेट पर सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया कि अन्दर मोबाइल ले जाना मना है। मैं ठहरा ‘इंजीनियर’। बात चुभ गई। अगले दिन फिर मोबाइल ले गया लेकिन स्विच ऑफ करके गेट पर ही रखना पडा। तीसरे दिन से जाना बन्द।
अब मैं खाली था। उधर रोहित जो सोना कम्पनी में साथ काम करता था, वो अभी भी वहीं था लेकिन भागने की फिराक में था। हम गुडगांव में राजीव नगर में रहते थे। अपने कमरे को नाम दे रखा था-
जाट धर्मशाला। इसके बारे में पहले लिख चुका हूं।
एक बार रोहित हरिद्वार गया एक प्रतिष्ठित कम्पनी में इंटरव्यू देने लेकिन असफल रहा। वहां उसकी दोस्ती ‘घटोत्कच’ से हुई। घटोत्कच भी उसी कम्पनी में इंटरव्यू देने गया था और तब गुडगांव में गैब्रियल नामक कम्पनी में काम करता था।
मुझे बेरोजगार देखकर घटोत्कच ने गैब्रियल में बात की। मामूली इंटरव्यू के बाद मेरी बेरोजगारी दूर हो गई।
यहां मेरी जिन्दगी का एक बेहतरीन समय बीता। इसके पुराने प्लांट से कुछ हटकर एक नया प्लांट बना था, बिल्कुल भी भीडभाड नहीं थी। इस प्लांट में दो मैनेजर थे। एक के अधीन तीन लडके थे और दूसरे के अधीन पांच छह लडके और इतनी ही लडकियां। मैं पहले वाले के अधीन था।
यहां बाइक के शॉकर की असेम्बली होती थी। आठ घण्टे में 240 शॉकर बनते थे जो कि मात्र चार घण्टे का काम था। शॉकर को असेम्बल करके एक विशेष प्रकार की ट्रॉली पर रखना होता था जो हमेशा सीमित संख्या में ही उपस्थित रहती थीं। यहां से ये ट्रॉलियां हीरो होण्डा के मेन प्लांट में जाती थीं। कभी कभी ये अगले दिन दोपहर तक वापस आती थीं, तो हम दोपहर तक खाली रहते थे।
चार घण्टे में 240 शॉकर फिट करके हम बिल्कुल फ्री होते थे। फ्री होने के बाद हम जो करते थे, उसी की वजह से यहां मन भी लगता था। सीधे दूसरे मैनेजर की कर्मचारियों के पास जा पहुंचते। हम सभी डिप्लोमा इंजीनियर ही थे। माहौल इतना दोस्ताना था कि अक्सर हम एक दूसरे के प्लांट में जाकर काम कर आते थे। कभी लडकियां हमारे साथ काम करती थीं तो कभी हम उनके साथ। मात्र 240 बनाओ और फिर कोई पूछने वाला नहीं। मैं पहले भी लिख चुका हूं कि इतने पीस बनाना चार घण्टे का काम था और हमारे पास इसके लिये आठ घण्टे थे।
यहां कैंटीन भी थी, जिसमें अपनी साथिनों के साथ बैठकर खाना खाने में आनन्द आ जाता था।
सुबोध कुमार- लडकियों का मैनेजर- उससे यह हजम नहीं हुआ कि दूसरे मैनेजर के ये लडके उसके प्लांट में आकर लडकियों से बात करें। वो अक्सर हमें टोकता रहता था कि इधर क्यों घूम रहे हो तो हमारा रटा रटाया जवाब रहता कि हमारा काम खत्म। उसे चुप हो जाना पडता था।
जब सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था तो एक पंगा हो गया। हमारा मैनेजर होली की छुट्टी चला गया। अब हमारा चार्ज भी सुबोध पर आ गया। मुझे भी होली पर मेरठ जाना था, तो 240 पीस बनाने के बाद तीन बजे मैंने उससे बाहर जाने के लिये गेट-पास मांगा। उसने मना कर दिया। मैंने कहा कि आज का टारगेट पूरा हो गया है, चार बजे ट्रेन है मेरठ के लिये। वो चूंकि हम तीनों से पहले से ही खार खाये बैठा था, मना कर दिया।
यह दूसरा मैनेजर मुझे जाने से रोक रहा है- मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मना करने के बावजूद बाहर चला आया। सुरक्षा गार्ड हमारी बडी इज्जत करता था, उसने कुछ नहीं कहा।
होली के बाद जैसे ही कम्पनी में घुसने लगा तो गार्ड ने रोक लिया। बोला कि साहब, सुबोध सर ने उस दिन मुझे बडी डांट लगाई थी आपकी वजह से। उन्होंने कहा है कि आपको अन्दर नहीं आने देना है। मैंने सुबोध से बात की तो उसने कहा कि जब तक अन्दर आने को कहा ना जाये, तब तक बाहर बैठो। यह मेरे लिये बडी करारी बात थी। पूरे दिन मैं बाहर बैठा रहा।
अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, तो मैंने ताव में आकर सुबोध को खूब गालियां सुना दीं। उसी दिन उस कम्पनी से मेरा पत्ता हमेशा के लिये कट गया।
यहां से निकाले जाने के बाद कई दिनों तक मैं बडा परेशान रहा। इसका एक कारण तो वे लडकियां ही थीं। देहरादून की लडकियां वैसे भी सुन्दर मानी जाती हैं। यहां भी देहरादून की कई लडकियां थीं। उन्हीं के कारण आठ घण्टे आठ मिनट की तरह लगते थे। दूसरा कारण काम का दबाव ना होना भी था। दिन का टारगेट पूरा करो, बस।
फिर एक रोजगार वाली वेबसाइट की मदद से गुडगांव में ही एक और कम्पनी सनराइज में गया। यहां भी अच्छा कम्पटीशन था और मात्र मेरा चयन हुआ था।
अब गर्मियां आने लगी थीं, और इस नई कम्पनी में मेरा काम था फोर्जिंग प्लांट की भट्टियों की देखभाल। फोर्जिंग प्लांट में लोहे को पिघलाने के लिये बडी बडी भट्टियां लगी होती हैं। दो दिनों में ही मेरा दिमाग चकरा गया। एक तो गर्मियां और ऊपर से भट्टियां। मैं चार दिनों तक नहीं गया। पांचवें दिन जब लगने लगा कि बेटा, अब बेरोजगारी सहन से बाहर की बात होती जा रही है। घरवाले भी तेरी ही तरफ हाथ फैलाये बैठे हैं, तुझे जाना ही पडेगा।
पांचवें दिन जब गया तो बॉस ने बुलावा भेजा। देखते ही उबलते दूध की तरह पतीले से बाहर हो गया। पन्द्रह मिनट तक नॉन-स्टॉप बुरी-बुरी सुनाता रहा। भट्टियों की गर्मी तो किसी तरह सहन हो जाती, लेकिन यह गर्मी सहन से बाहर की चीज थी। आखिर में उसने मेरे सामने एक कागज फेंककर चिल्लाते हुए कहा कि नौकरी नहीं करनी तो लिखकर दे दो। चुटकी में बाहर करवा दूंगा।
मैंने फैसला तो कर ही लिया था। यह बात सुनते ही कहा कि सर, बोलो, क्या क्या लिखना है। गजब का इंसान था वो भी। मेरे इतना कहते ही ऐसा हो गया जैसे फूले गुब्बारे में सुई चुभो दी हो। अभी तक जो गुब्बारा फूलता ही जा रहा था, अब अचानक पिचक गया।
प्यार से कहने लगा कि बेटे, आज के समय में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। तुम ही देखो, कितने लोग आये थे यहां नौकरी के लिये लेकिन मिली तुम्हें। यह तुम्हारे लिये एक मौका है, इसे जाने मत दो। लाओ, कागज मुझे दो और जाओ भट्टियों में।
मैंने शान्ति से कहा कि इस पर लिखना क्या है?
बोला कि कुछ नहीं लिखना। पुनर्विचार कर लो अपने फैसले पर।
मैंने कहा कि पुनर्विचार का पुनर्विचार भी कर लिया। आप कुछ नहीं लिखवाओगे, कोई बात नहीं; इस खाली कागज को मेरा रिजाइन ही समझना। और जाओ, अपनी तीन दिन की सैलरी भी नहीं लूंगा।
अब मैं फिर बेरोजगार था।
मैं अपनी ‘जाट धर्मशाला’ में पडा सोचता रहता। अपने घर का एकमात्र जिम्मेदार सदस्य था मैं और अपनी जिन्दगी इतनी गैर-जिम्मेदारी से गुजार रहा था। पिछले छह महीनों में मैं छह बार नौकरियां बदल चुका था। लगता कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। दूसरे पूछते तो कभी भी अपनी गलती नहीं बताई जा सकती थी, सारा दोष कम्पनी पर ही थोप देता था।
रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने की बडी तमन्ना थी और उसके लिये मैं भरसक कोशिश कर रहा था। सिकन्दराबाद और नागपुर में लिखित परीक्षा भी दे आया था लेकिन दोनों जगह असफल।
फिर फैसला किया कि हरिद्वार चलते हैं। गुडगांव के दोस्तों ने समझाया कि वहां इतना पैसा नहीं है, जितना कि गुडगांव में। मेरा कहना था कि पैसा गुडगांव में भी नहीं है। आखिरकार अगस्त में हरिद्वार चला गया।
एक प्लेसमेंट एजेंसी की सहायता से स्वर्ण टेलीकॉम में आवेदन किया। उन्हें एक ऐसे डिप्लोमची की जरुरत थी तो ऑटोकैड भी जानता हो। यानी कम्प्यूटर में कम्पनी के प्रोडक्ट की डिजाइन भी बना सके। मैंने यह कोर्स कर तो रखा था लेकिन लिया दिया ही किया था और इसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं था। जब उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने कहा कि सर्टिफिकेट से काम करवाओगे या मुझसे?
उन्होंने मुझे एक साधारण सा लोहे का टुकडा लाकर दिया। बोले कि इसकी डिजाइन कागज पर बनाओ। मैं मैकेनिकल डिजाइन का एक उत्कृष्ट विद्यार्थी था, इसलिये बडी आसानी से उसे कागज पर बना दिया। अब बोले कि इसे कम्प्यूटर में बनाओ। सालभर हो गया था कॉलेज छोडे हुए और कम्प्यूटर भी। फिर भी किस तरह मैं उसे बना पाया, मैं ही जानता हूं। आखिरकार वे मेरे काम से सन्तुष्ट हो गये।
अब मेरा काम था अपना हाथ कम्प्यूटर डिजाइन में अधिक से अधिक साफ करना। जल्दी ही मैंने उसमें अधिकतम सफलता प्राप्त कर ली। सैंकडों तरह के छोटे छोटे पीस यहां बनते थे, सब की डिजाइन मेरे पास थी। जब भी जिस किसी पीस की भी जानकारी चाहिये होती थी, दो मिनट में मिल जाती थी। अपने ‘डिपार्टमेंट’ का मैं ही कर्मचारी था और मैं ही बॉस। चूंकि ज्यादातर समय मैं खाली रहता था, लेकिन कम्प्यूटर और इंटरनेट होने की वजह से कभी बोर नहीं होता था।
उन्हीं दिनों 6 नवम्बर 2008 को अचानक
यह ब्लॉगबन गया, जिसने आज मुझे वैश्विक पहचान दी है।
मेरे आसपास जितने भी इंजीनियर थे, सभी ग्रेजुएट थे। उनकी सैलरी भी मेरी जितनी ही थी। इस बात की मुझे खुशी होती थी कि ग्रेजुएट इंजीनियरों की सैलरी भी मेरे बराबर है जबकि उन्हें यही बात चुभती थी। विजय कुमार था एक इसी तरह का इंजीनियर जिसने इसी चुभन से परेशान होकर अपना इस्तीफा लिख दिया था लेकिन कम्पनी के हुक्मरानों ने विजय को मना लिया, दो तीन हजार सैलरी भी बढ गई।
इसी विजय को एक बात और सर्वाधिक चुभती थी कि एक डिप्लोमची इंजीनियर पूरे दिन कम्प्यूटर पर बैठा रहे। उसने अपनी कुर्सी भी मेरे बराबर में लाकर रख दी ताकि बाहरियों को पता चले कि विजय भी कम्प्यूटर जानता है।
एक दिन विजय ने कम्पनी के सर्वेसर्वा जीएम से शिकायत कर दी कि नीरज इंटरनेट चलाता है। जीएम एक बूढा था, कान का कच्चा। मेरी अनुपस्थिति में इंटरनेट वाली केबल निकालकर ले गया। मैं आया, देखा कि नेट नहीं है, केबल नहीं है, तो आसपास बैठे मित्रों से पूछाताछी की तो विजय ने ही बताया कि जीएम साहब निकालकर ले गये हैं। मैं तुरन्त जीएम के यहां पहुंचा और सीधे केबल मांगी। जीएम ने कहा कि तुम करते क्या हो नेट से? मैंने कहा कि मैं बहुत बढिया काम करता हूं। नेट पर डिजाइनिंग की शानदार तकनीकें सीखता हूं, इससे गुणवत्ता में बढोत्तरी होती है। बुढऊ था ही कान का कच्चा, बोला कि हां तब तो तुम्हें नेट जरूर चलाना चाहिये। मैंने कहा केबल, बोला कि विजय के पास हैं, उससे ले लो। आखिरकार केबल विजय के लॉकर में मिलीं।
जब मेरा ब्लॉग बन गया, तो ज्यादातर समय उसी में लगने लगा। एक दिन मैं कोई पोस्ट लिख रहा था कि जीएम ने धमाकेदार एंट्री की। इस तरह वो पहले कभी हमारे यहां नहीं आता था, यह विजय की ही काली करतूत लगती है। जीएम सीधा मेरे सिर पर आकर खडा हो गया, बोला कि यह क्या लिख रहे हो हिन्दी में? मैंने कहा कि सर, सक्सेना साहब कह रहे थे कि कर्मचारियों के लिये कुछ प्रिंट आउट हिन्दी में चाहिये, जिसमें मशीन चलाने की सावधानियां लिखी हों। मैं उन्हें तैयार करने के लिये हिन्दी लिखना सीख रहा हूं। ... तो यह क्या है जाट धर्मशाला.. क्या है यह? मैंने कहा कि सर, सीखने के लिये कुछ ना कुछ ऊंट-पटांग तो लिखना ही पडेगा। बात उसके समझ में आ गई। बोला ठीक है।
अब मेरे कान खडे होने शुरू हो गये कि आगे आने वाला समय बडा भयंकर है। विजय से बात तो कभी की बन्द हो चुकी थी। गुणवत्ता के मामले में मैं था भी उत्कृष्ट। अब तक हाथ इतना जम चुका था कि कभी कभी अगर प्रोडक्शन और मार्केटिंग वाले मेरे पास बैठकर किसी नये प्रोडक्ट की बात करते तो उन्हें हाथों हाथ उस काल्पनिक प्रोडक्ट का थ्री-डी फोटो मिल जाता।
अब मुझे हर समय कम्प्यूटर में एक विंडो में डिजाइनिंग का पेज खोले रखना पडता था, पता नहीं कब जीएम का छापा पड जाये और नेट कनेक्शन हट जाये। इसी तरह एक दिन मैं डिजाइनिंग का पेज मिनिमाइज करके एक्सेल पर अपनी रेल-यात्राओं की गणना करने में मशगूल था, तो जीएम का छापा पड गया। छापा इतना जबरदस्त था कि एक्सेल को मिनिमाइज तक करके का समय नहीं मिला। मेरे सिर पर खडे होकर देखने लगा। एक्सेल शीट पर ट्रेनों के नाम, स्टेशन देखकर अपनी विजय और अपने विजय दोनों पर बडा इतरा रहा होगा कि नीरज को रंगे हाथों नेट का दुरुपयोग करते पकड लिया।
बोला कि यह क्या है?... सर, यह एक्सेल शीट है।... नेट पर तुम अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हो? तुम्हारा नेट अब से बन्द कर दिया जाता है। विजय से कहकर केबल हटा दी गई। अब मैंने कहा कि सर देखो, नेट पर तो मैं डिजाइनिंग का काम ही कर रहा था, यह जो आपने ट्रेन वगैरह देखी हैं, वे एक्सेल की करामात हैं, तो नेट कनेक्शन हटने के बाद भी चलता रहेगा। हालांकि उस पर कोई फरक नहीं पडा और मुझे नेट से महरूम होना पडा।
अब मेरे लिये सीधी सीधी घण्टी नहीं, घण्टा बज चुका था।
स्वर्ण टेलीकॉम एक छोटी सी कम्पनी थी। इसमें मुझे छोडकर बाकियों को कई कई काम करने पडते थे। एक थे मनपाल सिंह। उन्हें ज्यादातर सेल्स का काम देखना होता था लेकिन किसी नये का इंटरव्यू भी वही लेते थे और एक तरह से कम्पनी के सर्वेसर्वा बन गये थे।
एक दिन एक लडका वहां किसी सिफारिश से इंटरव्यू देने आया। कम्पनी में उसके लिये कोई जगह नहीं थी लेकिन सिफारिश होने की वजह से इंटरव्यू की फॉर्मलिटी पूरी करनी थी। मनपाल ने उसका इंटरव्यू लिया। आखिर में उससे कह दिया कि अभी हमारे बडे सर भी इंटरव्यू लेंगे, वे ही तुम्हें आगे की बतायेंगे।
मनपाल अपनी चिर-परिचित मुस्कान बिखेरता हुआ हमारे ऑफिस में आया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस ऑफिस में मुझ समेत कई इंजीनियर काम करते थे। मैं डिप्लोमची था, बाकी सभी ग्रेजुएट। आते ही मनपाल ने कहा कि यार, उधर एक बन्दा बैठा है। हमारे यहां जगह तो है नहीं, उसे किसी तरह यहां से टालना है। कौन जायेगा?
सर्वसम्मति से मुझे भेजा गया। तय था कि उससे कहना है कि दस पन्द्रह दिन में फोन करके बतायेंगे।
कल तक जहां मैं दूसरों के सामने याचक की तरह बैठकर इंटरव्यू दिया करता था, आज मैं ‘बडा अफसर’ बनकर इंटरव्यू लेने जा रहा था।
जाते ही उसका नाम पूछा, पढाई लिखाई की जानकारी ली। और जब देखा कि यह भी कम्प्यूटर डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट लिये बैठा है और इसके आने से मेरा ढोल बजना तय है तो मैंने सीधे सीधे कहा कि भाई, यहां तेरे लायक वैकेंसी ही नहीं है। तू ठहरा मैकेनिकल का बन्दा, यह कम्पनी है टेलीकॉम की, तो तेरा यहां कोई भविष्य भी नहीं है। यहां से चला जा, अपने फील्ड की ही कोई कम्पनी ढूंढ।
यहां रहते रहते गोरखपुर में दो बार और चण्डीगढ में एक बार रेलवे जेई का पेपर देने गया, लेकिन तीनों बार असफल। हिम्मत ने कभी हार नहीं मानी। और जब दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर की भर्ती की सूचना आई, तो यार लोगों ने कहा कि इसमें मात्र 11 सीटें ही हैं, लाखों धुरन्धर परीक्षार्थी आयेंगे, तू कहीं भी नहीं टिक पायेगा, तो उनकी इस अनमोल सीख का कोई असर नहीं पडना था।
उन लाखों में से करीब पचास परीक्षार्थी इंटरव्यू के योग्य पाये गये। इन पचास में मैं भी था।
यहां मुझे लगने लगा कि अब मैं आसानी से इंटरव्यू की बाधा से आगे निकल जाऊंगा। आखिर मैं पिछले डेढ साल से लगातार इंटरव्यू ही तो देता आ रहा था। मेरे लिये इंटरव्यू कोई हौव्वा ना होकर बिल्कुल साधारण सी बात हो चुकी थी।
आज दिल्ली मेट्रो में मुझे चार साल हो चुके हैं।